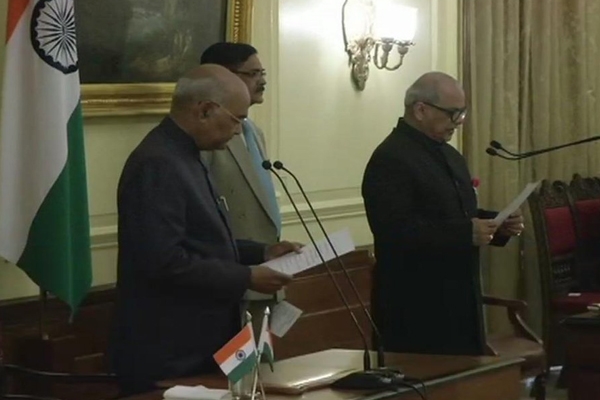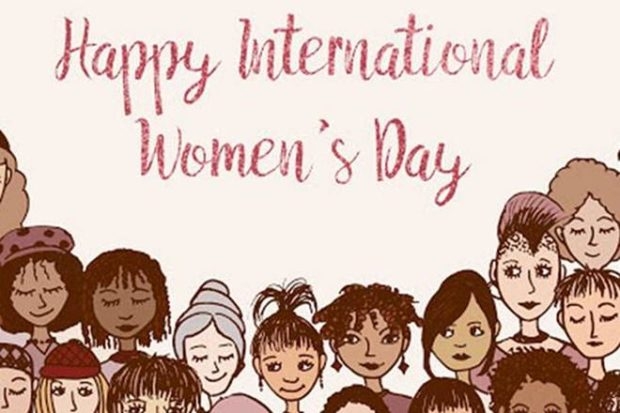डॉ. सुधीर सक्सेना
नाम आबिद हसन। पूरा नाम जैन-अल-आब्दीन हसन। निजामशाही के दौर में हैदराबाद में कुलीन घराने में पैदा हुथे। पहले इंडियन नेशनल आर्मी में रहे और फिर भारतीय विदेश सेवा में। अदब से लगाव था। शाइरी भी करते थे। खयालात इंकलाबी थे। भगवा रंग से अनुराग था, लिहाजा तखल्लुस रखा सफ़रानी। जाने-पहचाने गये आबिद हसन' सफरानी के नाम से।
बिला शक आबिद हसन साहब आला दर्जे की शख्सियत थे। उन्हें अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत थी। मादरे-वतन से मोहब्बत की रौ में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के निजी सचिव और आजाद हिन्द फौज में सक्रिय रहे। फिर बंदी बने और फिर राजनय में आकर मिस्र और डेन्मार्क में भारत के राजदूत रहे। मगर उनका महान और कालजयी योगदान है कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के आदेश पर उन्होंने 'जयहिन्द का बेमिसाल नारा गढ़ा और विश्व कवि रबीन्द्रनाथ ठाकुर कृत राष्ट्रगीत का अनुवाद किया। आज जयहिन्द देश में सुरक्षा और सैन्यबलों में अभिवादन का मान्य और व्यवहृत अभिवादन है। इसके पंचाक्षरों में राष्ट्रप्रेम की भावना तरंगायित है। वह जोश, जज़्बे, समर्पण और सम्मान की अभिव्यक्ति है। नेताजी ने इसे स्वीकारा और इसके लिये अपने जाँबाज सेनानी की पीठ थपथापायी थी। यही नहीं, स्वप्नदृष्टा प्रधानीमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने जब मध्यरात्रि में आजादी पर भारतीय संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो इसका उपयोग किया। भारत की प्रधानमंत्री रही, आयरन लेडी इंदिरा गांधी तो अपने भाषणों में अंत में अवाम से जयहिंद का नारा लगवाती थीं। कोकिल कंठी महान गायिका ने अपने गाये गीत में 'जयहिंद' को स्वर देकर इसमें प्राण फूँके थे। आज जयहिन्द की सेना का नारा आसेतु हिमाचल घर-घर गूंज रहा है और जन-जन में स्फूर्ति का संचार कर रहा है।
इसी जयहिन्द के रचयिता थे जनाब आबिद हसन। 11 अप्रैल, सन 1911 को हैदराबाद में जनने आबिद की माँ उपनिवेशवाद के सख्त खिलाफ थीं और पराधीनता को अनुचित मानती थीं। बालक आबिद पर मां की सीखों का खासा असर हुआ और उनके भीतर बर्तानवी हुकूमत के खिलाफ रोष धधकने लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जॉर्ज्स ग्रामर स्कूल में हुई। आगे पढ़ने की वेला आई तो माता-पिता ने अपने इंकलाबी खयालों के मद्देनजर आबिद को इंग्लैंड के बजाय जर्मनी भेजने का फैसला किया। ऐसे दौर में जब लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिये विलायत भेजते थे, आबिद को जर्मनी भेजना बहुत मायने रखता है। यकीनन इसके पीछे उनके जज्बे का हाथ था।
युवा आबिद हसन जब जर्मनी में इंजीनियरिंग के छात्र थे, उन्हें नेताजी सुभाष बोस को सुनने का मौका मिला। नेताजी वहां भारतीय बंदियों के समूह को संबोधित कर रहे थे। वह ब्रिटिश सत्ता को सशस्त्र क्रांति से उखाड़ फेंकने की योजना पर भी काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी आजाद हिन्द फौज का गठन इसी निमित्त किया था। नेताजी के ओजस्वी भाषण से आबिद बड़े प्रभावित हुये और कहा कि पढ़ाई पूरी कर वह उनके आंदोलन से जुड़ना चाहेंगे। इस पर नेताजी ने उन्हें टोका और कहा कि राष्ट्र भक्ति इंतजार नहीं करती। इसके लिये त्याग करना होता है। नेताजी की बात आबिद को लग गयी। फिर क्या था? उन्होंने पढ़ाई अधूरी छोड़ी। और नेताजी से जुड़ गये। नेताजी ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया। वह उनके दुभाषिया भी हो गए। नेताजी के जर्मनी प्रवास में आबिद उनके दुभाषिये के तौर पर सक्रिय रहे। प्रसंगवश बता दें कि आबिद शब्द का अर्थ होता है अनुयायी या उपासक। आबिद सही अर्थों में नेताजी के अनुयायी व उपासक थे। वह उनकी इंगित पर प्राण निछावर करने को तत्पर थे।
द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ चुका था। नेताजी की दृष्टि में यह ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकेने का सुनहरा मौका था। हसन नेताजी के अत्यंत विश्वास-पात्र थे। सन 1943 में नेताजी जब जर्मन यू बोट -यू 180 से दक्षिण-पूर्व एशिया की लंबी यात्रा पर गये तब आबिद उनके साथ थे। दरअसल, यू-180 एक जर्मन पनडुब्बी थी और उससे नेताजी समुद्री मार्ग से अपने मिशन के तहत जापानी अधिकारियों से मिलने गये थे। अभियान सफल रहा। नवगठित आईएनए यानि आजाद हिन्द फौज ने सामरिक मोर्चे पर उल्लेखनीय सफलताएँ अर्जित कीं। भारत का एक हिस्सा स्वतंत्र हुआ। आबिद अब एक फौजी थे; स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। आजाद हिन्द फौज में वह मेजर बने। यह वह दौर था, जब उन्होंने 'सफरानी' उपनाम अपनाया। उनकी नजरों में सैफ्रन' (भगवा) रंग द्वेष या घृणा का रंग न होकर प्रेम का पवित्र रंग था।
यह व दौर था, जब फौज में अभिवादन के लिये अनेक संबोधन प्रचलित थे। कोई राम-राम कहता था, कोई सतश्री अकाल तो कोई सलाम वालेकुम। नेताजी एकरूपता चाहते थे। हर जाति-धर्म के लिए एक ही संबोधन। उन्होंने साथियों से टकली-शब्द गढ़ने को कहा। ठाकुर यशवंत सिंह ने हिन्दुस्तान की जय' का सुझाव दिया, लेकिन हरफनमौला आबिद ने खरी गिन्नी सा सुनहरा शब्द पेश किया : 'जयहिन्द।' जयहिन्द सबको भा गया। नेताजी ने तुरंत सहमति दी। कहने की जरूरत नहीं कि आज यह शब्द विश्वव्यापी अहमियत रखता है।
जनाब आबिद के फन का कमाल यहीं तक सीमित नहीं है। आजादी की लड़ाई में बंकिमचन्द्र के 'वंदेमातरम्' का अतुल्य योगदान रहा, अलबत्ता धार्मिक कारणों से उस पर कुछ आपत्तियां भी आयीं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने 'जनगणमन' लिखा और उसे कंपोज भी किया। कांग्रेस के अधिवेशनों में सामूहिक तौर पर गाया गया, लेकिन इसकी संस्कृत निष्ठता नेताजी को अखरती थी। यद्यपि कैप्टेन लक्ष्मी सहगन व अन्य इसके पक्ष में थे, लेकिन नेताजी ने आबिद से इसका सरल-सुबोध तर्जुमा करने को कहा। उन्होंने बड़ी संजीदगी और मेहनत से गीत प्रस्तुत किया: शुभ सुख चैन। नेताजी बड़े प्रसन्न हुये। उन्होंने रामसिंह ठाकुर से इसकी धुन बाँधने को कहा। एक ऐसी धुन जिसे फौजी कूच के मौके पर बजाया जा सके। रामसिंह ने ऐसा ही किया। इसे भारत के प्रोवीजनल (अनंतिम) राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता मिली। अंततः सन 1950 में जन गण मन को बतौर राष्ट्र गान को वैधानिक मान्यता से 'शुभ सुख चैन की बरखा बरसे का क्रम टूटा।
विश्व युद्ध की समाप्ति पर आबिद समेत आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा चला, जिनकी पैरवी स्वयं पं. नेहरू ने की। सन 1946 में रिहाई पैरवी के बाद वह अपने गृहनगर हैदराबाद चले आये, किंतु जल्द ही वह नवजात भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) में शामिल हो गये। बतौर राजनयिक उनका करियर चमकीला रहा। वह मिस्र और डेन्मार्क में राजदूत बने। सन 1969 में' सेवानिवृत्ति पर वह फिर हैदराबाद लौट आये। उनकी भतीजी सुरैया हसन ने नेताजी के भतीजे अरबिन्दो बोस से शादी की और सफल जीवन बिताया। सुरैया आबिद के बड़े भाई बदरूल हसन की बेटी थी; जिन्होंने राष्ट्रपिता गाँधी के साथ काम किया था। अंतिम बरसों में जनाब आबिद का अधिकांश समय उर्दू-फारसी कविता के साथ बीता।
जनाब आबिद हसन 'सफरानी अब नहीं है। 9 अप्रैल, 1984 को हैदराबाद में उनका इंतकाल हो गया और उन्हें वहीं सुपुर्दे खाक किया गया। 'जय हिन्द' का यह रचयिता हमारे सम्मान का हकदार है। आइये, उसे सलाम करते हुये हम कहें : जयहिंद। जनाब आबिद हसन 'सफरानी।








359.jpg)



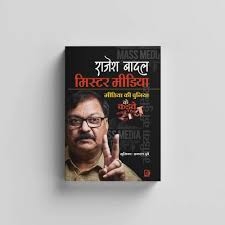
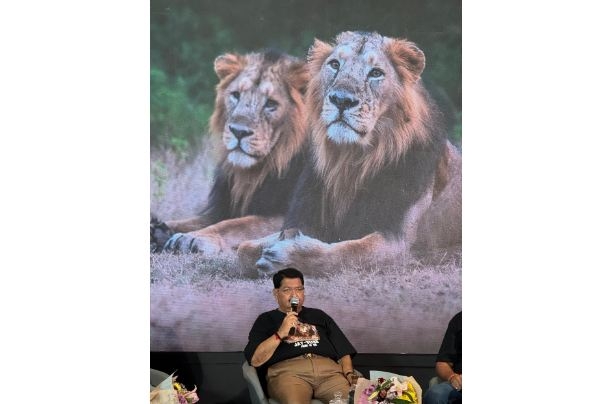
19.jpg)
32.jpg)
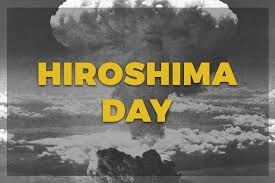
16.jpg)